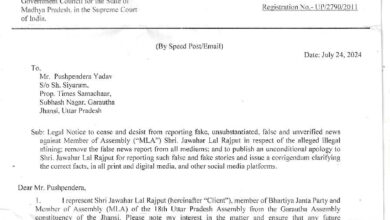विज्ञापन बंद कराइए, पर चेहरा कहाँ छुपाइए?
![]() लेखक: एक व्यथित पर विनोदी पत्रकार
लेखक: एक व्यथित पर विनोदी पत्रकार
एक दिन सूचना निदेशक महोदय के कार्यालय में एक महानुभाव पहुँचे। विशेषता ये कि वो ‘मान्यता प्राप्त’ पत्रकार हैं, यानी सरकारी रजिस्टर में नाम दर्ज है, और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास कि जैसे राष्ट्र की पत्रकारिता उन्हीं के कंधों पर टिकी हो।
आते ही बोले —
“निदेशक महोदय, मासिक पत्रिकाओं का विज्ञापन बंद कर दीजिए। बहुत हो गया ये खर्चा-पानी। सबको पैसे बाँट रहे हैं, हम जैसों को क्या मिला?”
अब बेचारे निदेशक महोदय तो असमंजस में पड़ गए। सोचे — “ये तो वही हैं जो हर महीने विज्ञापन के लिए सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाते थे। अब क्या मिर्ची लगी?”
दरअसल बात कुछ और थी।
जैसे ही उनकी ये ‘देशहितकारी’ बात पत्रकार समाज को पता चली, तो भयानक कोहराम मच गया।
“अरे भइया, तुम्हारी कौन सी पत्रिका छपती है जो दूसरों का विज्ञापन बंद कराने चले आए?”
“तुम्हारी तो छपाई भी फेसबुक पोस्ट से ज्यादा नहीं टिकती!”
और फिर जो फजीहत हुई, वो इतिहास के पन्नों में सुनहरी स्याही से नहीं, लाल मुंह और झुकी निगाहों से लिखी गई।
जिस कॉफी हाउस में रोज गाल बजाते थे, वहाँ कुर्सी तक छीन ली गई।
जहाँ पहले ‘वरिष्ठ पत्रकार’ कह कर सम्मान मिलता था, अब लोग कहते हैं —
“वही हैं ना जो दूसरों की थाली में छेद करके खुद भूखे रह गए?”
कुछ पत्रकारों ने तो सुझाव भी दे डाला —
“इनको एक नया पुरस्कार मिलना चाहिए — ‘विज्ञापन विनाशक सम्मान’।”
और हमारे महानुभाव? अब हर जगह कहते फिरते हैं —
“मेरे कहने का मतलब वो नहीं था… मुझे तो गलत समझा गया…”