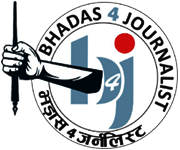जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब तक क्यों नहीं हुई FIR, क्या है वी रामास्वामी केस, क्यों सारी शक्ति CJI के हाथ: जानिए सब कुछ
किसी जज के खिलाफ शिकायत भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति को दी जा सकती है। अगर शिकायत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति को दी जाती है तो वे उस शिकायत को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भेजते हैं। CJI को लगता है कि शिकायत गंभीर नहीं है तो वे उसे खारिज कर सकते हैं।
 दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर लगी आग में होली के दिन बड़ी मात्रा में अघोषित नकदी मिली थी। इस नकदी की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसको लेकर लोगों में सवाल उठा कि इतनी भारी मात्रा में नकदी मिलने के बावजूद इस मामले में FIR क्यों नहीं की गई। जस्टिस वर्मा पर FIR करने की माँग वाली एक याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आइए जानते हैं, इसके पीछे क्या वजह है।
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर लगी आग में होली के दिन बड़ी मात्रा में अघोषित नकदी मिली थी। इस नकदी की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसको लेकर लोगों में सवाल उठा कि इतनी भारी मात्रा में नकदी मिलने के बावजूद इस मामले में FIR क्यों नहीं की गई। जस्टिस वर्मा पर FIR करने की माँग वाली एक याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आइए जानते हैं, इसके पीछे क्या वजह है।
इस सवाल का उत्तर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में निहित है, जो अब एक कानूनी ढाँचे का रूप से ले लिया है। यह वी. रामास्वामी बनाम भारत संघ (1991) मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से उपजा है, जिसके कारण जजों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होने का निर्णय लेने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के हाथों में आ गया है।
इस फैसले के बाद CJI तय करेंगे कि जिस जज पर आरोप लग रहा है कि वह आपराधिक कदाचार या अक्षमता है या नहीं है। अगर है भी तो CJI के सहमति के बाद भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए सकता है। यानी सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश जज पर लगाए गए आरोपों का आकलन करेंगे।
इसके बाद ही CJI राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि उस जज के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। हालाँकि, शीर्ष न्यायालय ने माना था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जज भी ‘लोक सेवक’ हैं। इसलिए लोक सेवक होने के नाते जजों पर भी आय से अधिक संपत्ति रखने जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन, सब कुछ CJI के हाथ में होगा
जस्टिस रामास्वामी बनाम भारत संघ
जस्टिस रामास्वामी मामले में शीर्ष न्यायालय ने तर्क दिया था कि यह तंत्र न्यायिक स्वतंत्रता को जवाबदेही के साथ संतुलित करता है। बाद में इसी फैसले को और अधिक परिष्कृत किया गया। सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति एएम भट्टाचार्जी (1995) मामले में जजों के खिलाफ मिली शिकायतों की जाँच के लिए ‘इन-हाउस प्रक्रिया’ को औपचारिक रूप से दिया।
सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति एएम भट्टाचार्जी (1995) में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 124 के तहत ‘बुरे व्यवहार’ और ‘महाभियोग योग्य दुर्व्यवहार’ के बीच अंतर को स्पष्ट किया। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने न्यायिक कदाचार की जाँच के लिए एक ‘आंतरिक प्रक्रिया’ के तहत पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने अक्टूबर 1997 में अपनी रिपोर्ट दी और सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1999 में इसे अपनाया।
साल 2014 में इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसमें संशोधन किया। साल 2014 में मध्य प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके गंगेले बनाम रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश मामले में आंतरिक प्रक्रिया में संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेएस खेहर और अरुण मिश्रा ने सात चरण वाली प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की।
इसके तहत, किसी जज के खिलाफ शिकायत भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति को दी जा सकती है। अगर शिकायत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति को दी जाती है तो वे उस शिकायत को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भेजते हैं। CJI को लगता है कि शिकायत गंभीर नहीं है तो वे उसे खारिज कर सकते हैं।
समीक्षा के बाद CJI एक जाँच समिति का गठन करते हैं। यह समिति तीन सदस्यीय होगी, जिसमें दो अलग-अलग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे। यह समिति न्यायाधीश से स्पष्टीकरण माँगती है। तमाम जाँच के बाद यह समिति CJI को अपनी रिपोर्ट देती है। इसमें बताया जाता है कि आरोपों में दम है या नहीं। साथ ही कदाचार के कारण निष्कासन कार्यवाही की आवश्यकता है या नहीं।
यदि कदाचार गंभीर नहीं हैतो CJI न्यायाधीश को सलाह दे सकते हैं और रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रख सकते हैं। यदि कदाचार गंभीर है तो CJI संबंधित न्यायाधीश को इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने की सलाह देते हैं। यदि आरोपित न्यायाधीश इससे इनकार करता है तो CJI संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश देते हैं कि आरोपित जज को न्यायिक कार्य सौंपना बंद दें।
यदि आरोपित न्यायाधीश फिर भी इस्तीफा नहीं देता हैं तो CJI राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित करते हैं तथा उन्हें हटाने की कार्यवाही की सिफारिश करते हैं। इसके बाद संसद में उस न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। हालाँकि, यह तमाम आंतरिक प्रक्रिया का जिक्र संविधान में नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजों के लिए खुद ही विकसित कर दिया गया है।
जस्टिस यशवंत वर्मा का केस भी इसी प्रक्रिया के तहत
जस्टिस यशवंत वर्मा का केस इसी ढाँचे के तहत प्रक्रिया में है। मामला सामने आने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को उनके गृह हाई कोर्ट इलाहाबादा भेजने का फैसला सुना दिया। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही दिल्ली हाई कोर्ट में लाया गया था। वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है।
CJI ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय से फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट माँगी। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने 25 पन्नों की रिपोर्ट CJI दी, जिसमें कहा गया कि मामले की गहन जाँच की जरूरत है। इसके बाद CJI ने जस्टिस डीके उपाध्याय को आदेश दिया कि वे जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य ना सौंपे। फिर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरण का आदेश निकाल दिया गया।
रिपोर्ट मिलने के बाद CJI खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की ‘आंतरिक जाँच’ कराने का निर्णय लिया। इस जाँच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। इस समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया जज वर्मा पर FIR की माँग वाली याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकारी परिसर में अवैध नकदी मिलने के मामले में FIR दर्ज करने की माँग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि याचिका समय से पहले दायर की गई थी। पीठ ने कहा कि CJI के निर्देश पर मामले की इन-हाउस जाँच जारी है।
दो जजों की खंडपीठ ने आगे कहा, “इन-हाउस जाँच पूरी होने के बाद कई विकल्प खुले हैं। सीजेआई एफ़आईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं या रिपोर्ट की जाँच करने के बाद मामले को संसद को भेज सकते हैं। आज इस याचिका पर विचार करने का समय नहीं है। इन-हाउस रिपोर्ट के बाद सभी विकल्प खुले हैं। याचिका समय से पहले है।”
याचिकाकर्ता नेदुम्पारा ने अपनी याचिका में कहा था कि केरल हाई कोर्ट के तत्कालीन जज के खिलाफ POCSO मामले का आरोप था, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि जाँच करना कोर्ट का काम नहीं है। इसे पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन-हाउस कमिटी वैधानिक प्राधिकरण नहीं है। यह विशेष एजेंसियों द्वारा की जाने वाली जाँच का विकल्प नहीं हो सकती है।
नेदुम्पारा ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में आम आदमी कई सवाल पूछ रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि 14 मार्च को जब नकदी बरामद हुई, उस दिन से आज तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? जब्ती का कोई पंचनामा क्यों नहीं बनाया गया? एक सप्ताह तक इस घोटाले को क्यों छिपाया गया? आपराधिक कानून क्यों नहीं बनाया गया? हालाँकि, पीठ ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।